INDIAN FUSION
WESTERN WEAR
LINGERIE & SLEEPWEAR
BEAUTY & PERSONAL CARE
JEWELLERY
FOOTWEAR
Original price was: ₹200.00.₹175.00Current price is: ₹175.00.
दिलीप मंडल Dilip Mandal ( Author )
Original price was: ₹200.00.₹175.00Current price is: ₹175.00.
Out of stock
‘हमारी जनगणना, हमारा भविष्य’- जनगणना में जाति : यथार्थ और विभ्रम
2011 की भारतीय-जनगणना का नारा है-‘हमारी जनगणना, हमारा भविष्य’. लेकिन ‘हमारी जनगणना’ हमारी समग्र पहचान को रेखांकित नहीं करती. वह ‘जाति’ नाम की कड़वी सच्चाई की समग्र पड़ताल से मुँह चुराती है. ऐसे में जिस जातिविहिन-समाज का भविष्यगामी-स्वप्न हमने संजोया है, उसके निर्माण आधार क्या होगा? क्या जातिवार-जनगणना इसके विश्वसनीय आँकड़े जुटाने की दिशा में अधिक प्रगतिशील और स्थाई कदम नहीं हो सकती? जन-प्रयासों और सामूहिक दबाव द्वारा यह संभव है न कि यथास्थितिवादी और प्रतिक्रियावादी सरकार या व्यवस्था से अपेक्षा करने से. वंचितों के सामूहिक प्रयासों और उनकी सकारात्मक माँगों को भरमाने की साजिश की ओर संकेत करती है. व्यवस्था के चरित्र को समझने में जब एक समाजशास्त्री ही मात खाने लगे तो आम-आदमी की बात ही क्या! बहरहाल जनगणना केवल ‘डाटा-संग्रहण’ भर न होकर एक महत्त्वपूर्ण अवसर है देश की सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-शैक्षणिक संरचना की सही समझ के निर्माण का ताकि अब तक की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की उपलब्धियों और कमियों की दशा और दिशा को जाना-जाँचा-पड़ताला जा सके. जनगणना में अपने समय व समाज की जरूरतों के मुताबिक आँकड़ों की व्यापकता या फैलाव का भी अपना महत्त्व है, वह उसे समृद्ध करता है, उसकी विश्वसनीयता को समय-दर-समय प्रासंगिक बनाता है. लेकिन हमारे देश की जनगणना आजादी के बाद से ही अपने समाज की सबसे क्रूर हकीकत ‘जाति’ (जन्म-आधारित स्थाई संस्था) के अस्तित्त्व तक से इनकार करती रही हैं. ‘जाति’ हमारे समाज की स्थाई और अखिल भारतीय बुराई है यह सभी मानते रहे है. ऐसे में इसकी समाप्ति के स्थाई-समाधानों की तलाश करने के बजाए इसके अस्तित्त्व तक से इनकार समझ से परे है जबकि किसी भी समस्या के मूल कारणों को जाने बगैर उसका इलाज संभव नहीं है. हमारे यहाँ आखिरी जातिवार-जनगणना 1931 में अंग्रजों के शासनकाल में हुई, तब पाकिस्तान और बाँग्लादेश भारत के अंश थे. द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण 1941 की जनगणना नहीं हुई और अगली (1951 की) जनगणना स्वतंत्रता के बाद हुई लेकिन हमारे शासकों ने पुन: जातिवार-जनगणना की कोई जरूरत नहीं समझी. यानि केवल सत्ता बदली सत्ता का चरित्र नहीं बदला.
| Price | |
|---|---|
| Language | |
| Writher & Author | |
| Book Condition | |
| Book Format |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
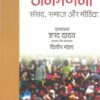
Out of stock
Reviews
There are no reviews yet.